
मुक्ति पर इतना विवाद,
खुलेपन पर इतना हंगामा क्यों ?
युग बीते, पर
क्या तुम्हारी लोभ से ललचायी आँखों से
पूर्व-राग का नशा नहीं उतरा ?
शाश्वत कुंठा या कायरता
हो गयी न अभिव्यक्त !
संस्कार दुबक गया
शिक्षा का, समाज का
जग गई न निसर्ग की सोई भूख
हो गये न ’पुरुष’
जिसे स्त्री का उन्नयन नहीं,
मनस-पूजन नहीं
देंह-गठन, त्वचा-संवेदन चाहिए !
मैं आवरण में थी
बस इसलिये ही
कि निरावृत होकर
नहीं करना चाहती थी
निखिल सृष्टि का सौन्दर्य मलिन,
रूप को ढांक-छिपा रखना चाहती थी
माया-मेघ की ओट
कि पुरुषत्व के जीवन में
भर न जाय ग्लानि,
मुक्ति का स्वर्ग-द्वार
रखती थी बंद सदा
कि उसकी झलक से संसार का कतृत्व
मोहांध विमुख न हो जाय ,
कंठ में ही
ठहरा देती थी अपना संगीत
कि उसकी चाह में मतवाले बन
तुम छानो ख़ाक
क्षिति-तल की,
अघा न जाओ तत्क्षण !
पर मेरे इस निष्पाप मनोयोग की
खूब परीक्षा ली है तुमने,
नग्न शरीर की शारीरिकता पर उलझे हो,
उसके पीछे की सारभावना भुलाकर ।
पर, अब
अतीत की नियति-रेखाओं को लुप्त कर
मैं नव्य-जीवन की राह लूँगी,
सच की आधारशिला पर गढूँगी
नव नन्दन-वन,
खुद के रूप पर रीझूँगी नहीं
मुक्त करूँगी स्वयं को
’खुद’ के कारागृह की दीवार तोड़,
विचरूँगी तितली-सी आनन्द-स्वच्छंद,
मधुहास-सी खिलूँगी,
बदलूँगी वस्तु का सन्दर्भ
(क्योंकि बदलता है न
सन्दर्भ-भेद से अर्थ !)
और तत्त्व-मुक्त दीख पड़ूँगी…
मतलब..
तब ’नारी’ हो जाउँगी
पूरक प्रेरणा भी, चुनौती भी !


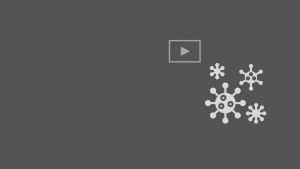



bahut sunder himanshu
पर मेरे इस निष्पाप मनोयोग की
खूब परीक्षा ली है तुमने,
नग्न शरीर की शारीरिकता पर उलझे हो,
उसके पीछे की सारभावना भुलाकर ।
शायद इसी अह्म ने नारी को बदलने के लिये मजबूर किया। बहुत अच्छी लगी रचना धन्यवाद्
बहुत सुंदर !!! विशेषतः यह—
मुक्ति का स्वर्ग-द्वार
रखती थी बंद सदा
कि उसकी झलक से संसार का कतृत्व
मोहांध विमुख न हो जाय ,
कंठ में ही
ठहरा देती थी अपना संगीत
कि उसकी चाह में मतवाले बन
तुम छानो ख़ाक
क्षिति-तल की,
अघा न जाओ तत्क्षण !
—-आपसे सदैव ऐसी ही अपेक्षा रहती है हिमांशु. साधुवाद !!!
agar NARI, Nari ke roop me aa gayi to phir MAHILA DIVAS manane ki jaroorat nahi hogi… bahoot khoob Sir…verma
हिमांशु जी बहुत गंभीर और चिंतनपरक रचना लगी – फुर्सत से एक बार फिर पढना पड़ेगा तब शायद ठीक से समझ पाउँगा.
बहुत सुंदर….. नमन….नमन…..
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.
himanshu ji
bahut hi sundarta se aapne nari ke astitva ko ukera hai……….ek sashakt rachna…….sashakt lekhan………naman hai.
मैं आवरण में थी बस इसलिये ही
कि निरावृत होकर नहीं करना चाहती थी
निखिल सृष्टि का सौन्दर्य मलिन….
क्षिति-तल की,
अघा न जाओ तत्क्षण !…
नग्न शरीर की शारीरिकता पर उलझे हो,
उसके पीछे की सारभावना भुलाकर …
कि तब नारी हो जाउंगी …पूर्ण प्रेरणा भी …चुनौती भी …
बहुत बढ़िया …
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बेहतर सौगात …!!
पौरुष की उद्दामता इसी में है कि उसमें कुछ अंश ही सही -कृष्ण सरीखी स्त्रैणता /स्त्री सख्यपन मौजूद हो -इस कविता में वह साफ़ ही झलकता है -अन्यथा यह क्यूकर हुआ की नारी अंतस की इतनी सटीक अनुभूति एक पुरुष -अभिव्यक्ति में समाहित हो आयी ? और पुनर्जन्मों का सिद्धांत जिस पर पूरा हिन्दू चिंतन ही मानो अवस्थित है सहसा ही सही लगने लगा -एक ही मन किसी जन्म में नारी और किसी में पुरुष ……और चेतना भावभूमि का भी स्थानान्तरण भी तदनुसार ही …वाह हिमांशु आपने तो जैसे निःशब्द ही कर दिया है .
मगर कविता सहज ही उपज जाय तो वही श्रेष्ठ भी है और अभीष्ट भी -कहीं कहीं यह वेगवती नदी तुल्य कविता किनारों के कचरे को भी लपेटती लग रही है पर क्या करियेगा नदी का स्वभाह ही है कलुष को धो डालना !
कहीं कहीं यह वेगवती नदी तुल्य कविता किनारों के कचरे को भी लपेटती लग रही है पर क्या करियेगा नदी का स्वभाह ही है कलुष को धो डालना !
—- sahee kahaa..aravind jee…….YAHI NARI HAI……
खुद के रूप पर रीझूँगी नहीं
मुक्त करूँगी स्वयं को
’खुद’ के कारागृह की दीवार तोड़,
विचरूँगी तितली-सी आनन्द-स्वच्छंद,
मधुहास-सी खिलूँगी,
बहुत सुन्दर हिमांशु ….मंत्रमुग्ध कर दिया इस कविता ने…कोई कवि मन ही नारी-मन को इतनी अच्छी तरह समझ सकता है….
और चित्र तो बस…ऐसा कि बस निहारते ही रहो…बहुत अच्छा लिखा है..
हिमांशु जी,
इधर कुछ दिनों से मन बहुत उद्विग्न रहा…परन्तु आज आपकी कविता ने हाथ पकड़ कर खड़ा कर दिया …एक सच्चा इन्सान वो होता है जो किसी भी जीव की वेदना को समझ पाता है और उसे व्यक्त कर पाता है और वही मनुष्य एक सच्चा कवि बन जाता है…भ्रमर गीत', मेघदूत जैसी कालजयी रचनाएँ कविमन की मात्र कल्पना नहीं है ये तभी बन पाईं हैं जब कवि ने इन जीवनों को जी लिया है…वेदना का संसार जब कविमनमें समाहित होता है तभी ऐसी अमूल्य कृतियाँ बनती हैं….आप सचमुच एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, कविराज हैं…
अगर आपको 'स्त्रैण' भी कहा जाए जो आप अपमानित मत होइएगा…क्योंकि कृष्ण को भी यही कहा गया था…
आपको नमन है 'कविराज'..
आपको पढ़कर प्रायः निशब्द हो जाता हूँ.. कभी अच्छे से समझता नहीं तो कमेन्ट नहीं कर पाता,कभी समझ जाता हूँ तो 'अवाक' रह जाता हूँ…!
अदा जी ने लिखा ..
इधर कुछ दिनों से मन बहुत उद्विग्न रहा…परन्तु आज आपकी कविता ने हाथ पकड़ कर खड़ा कर दिया..
यह तो मैंने भी महसूस किया है कि कविता में बड़ी शक्ति होती है. कई बार व्यथित मन इसे पढ़कर संभलता है…हाँ कविता में शक्ति होनी चाहिए. आपकी यह कविता अपने आप में सम्पूर्ण व कालजयी है.
माँ सरस्वती की असीम कृपा है आप पर जो उन्होंने नारी मन की अभिव्यक्ति के लिए आपको चुना.
…बधाई हो 'कविराज'.
shashakt rachna.
भई थकित मति चकित हमारी !
नारी मुक्ति को सही अर्थों में पहचाना है आपकी इस कविता ने। सहमत हूँ आपकी भावनाओं से।
हिमांशु जी,
नारी मन की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है इस कविता में। शरत बाबू की याद आ गई। केवल युग सन्दर्भ बदले हैं। आभार!
बहुत अच्छी रचना….बधाई
"’खुद’ के कारागृह की दीवार तोड़" गहन चिंतन से निकली बातों से असहमत कैसे हुआ जा सकता है भला !
Is behad khubsurut bhavo se saji sundar prastuti ke lie aapko bahut dhanywaad!
सुंदर रचना..आशा है कि विचारों के रास्ते उतर कर कई हृदयों मे अनुनादित होगी..जहाँ इसकी आवश्यकता भी है…
Via E-mail.
मैं तो चित्र पर ही अटक गया बन्धु!
खुले समुद्र का किनारा
पृष्ठभूमि में उग्र सी लहरों की कालिमा
डूबता सूरज
जींस टॉप पहने केश खोले युवती
पानी को पीट उछालती है –
आओ लहरों! डूबते सूरज की सखियों !!
तुम्हारी खैर नहीं –
ये पैर का ठेंगा तुम्हारे साथी सूरज के लिए
अंतिम लात उमंग भरी – डूबो जल्दी ..
मुझे परवाह नहीं –
न समझ आए तो मेरी देह भाषा पढ़ो।
यह चित्र कविता है।
और कविता ? – प्रतिध्वनि है।
@ ''जग गई न निसर्ग की सोई भूख
हो गये न ’पुरुष’
जिसे स्त्री का उन्नयन नहीं,
मनस-पूजन नहीं
देंह-गठन, त्वचा-संवेदन चाहिए !''
……………
निसर्ग की सोई भूख कभी अ-नैसर्गिक कृत्य
नहीं करती —
'' नव हो जगी अनादि वासना
मधुर प्राकृतिक भूख सामान ! ''( प्रसाद जी )
इस भूख को सकारात्मक पक्ष के रूप में देखा जाना चाहिए , पर
यह भूक जब अधिकार – सुख के साथ आती है तब बर्बर और
अ -नैसर्जिक हो जाती है ! यह स्थिति हेय, त्याज्य है !
.
जब भूख को निसर्ग शब्द के साथ आप रख रहें हों ( जैसा आपकी
कविता में है ) तो इस भूख को सकारात्मक अर्थ में लो मित्र ! क्या बुरा है !
.
बाकी टोंकार क्या करूँ !
टोंकार ही रह गया जो फटे नगाड़े जैसा बजता है अब भी , उस्तादी कहाँ रही अब !
'' अब न रहे वे पीने वाले / अब न रही वह मधुशाला ! ''
Himanshu ji,
Million people, zillion opinions !
Even the definition of 'nari mukti' is different in everyone's mind.Women may unite when it comes to 'nari mukti' but are they really united when they truly find a mukt woman? Likewise men unite when it comes to condemn the women lot. Anyways exceptions are always there. wonderful men and women are always around us.That helps us survive the bitter truth of life.
We need more GEMS like you with such beautiful thinking. Congrats for writing such a wonderful poem.
@ Amar ji,
बाकी टोंकार क्या करूँ !
टोंकार ही रह गया जो फटे नगाड़े जैसा बजता है अब भी , उस्तादी कहाँ रही अब !
'' अब न रहे वे पीने वाले / अब न रही वह मधुशाला ! ''
Nothing ends ! Life moves on !
Andar ka basant kabhi marta nahi,
Sachhai(honesty) ka sammaan karne wale abhi baaki hain.
"Nar ho na niraash karo mann ko….."
kaun rota hai kisi ki baat par yaron,
sabko apni hi kisi baat pe rona aaya…
बहुत सुंदर….. नमन….नमन…..