ऋग्वेद में वर्णन आया है : ‘शिक्षा पथस्य गातुवित’, मार्ग जानने वाले , मार्ग ढूढ़ने वाले और मार्ग दिखाने वाले, ऐसे तीन प्रकार के लोग होते हैं। साहित्यिकों की गणना इस त्रिविध वर्ग में होती है। सबसे अधिक योग्यता मैं उनकी मानता हूँ जो मार्ग ढूंढ़ने वाले होते हैं, जो नये मार्ग खोजते हैं, बहुत हिम्मत से आगे बढ़ते जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानव संवेदना की अटवी में कुछ ऐसे ही मार्ग-संधानकर्त्ता की पृष्ठभूमि रचने वाले साहित्यकार हैं जहाँ है सब के केन्द्र के मनुष्य, उसका संघर्ष, उसकी जिजीविषा और ‘मानव तुम सबसे सुन्दरतम’ की अप्रतिहत आस्था। अशोक के फूल की ये पंक्तियाँ द्विवेदी जी के मानवीय संवेदना के चितेरे होने का प्रतिफलन ही तो हैं-
‘‘समूची मनुष्यता जिससे लाभान्वित हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके प्रेम करे, एक समूह दूसरे समूह को दूर रखने की इच्छा न करके पास लाने का प्रयत्न करे, कोई किसी का आश्रित न हो, कोई किसी से वंचित न हो। इस महान उद्देश्य से ही हमारा साहित्य प्रणोदित होना चाहिये।’’
मानव संवेदनाओं के सहभागी के रूप में, उसके चितेरे साहित्यकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी यह उद्घोषित करते हुये दीखते हैं कि जीवन किस प्रकार का है, यह हमें नहीं देखना चाहिये। जहाँ उत्तम जीवन है, वहीं उत्तम विचार संभव है -यह तो सामान्य नियम हुआ। लेकिन किसी कारण अन्दर अन्दर एक चिन्तन प्रवाह होता है, तद्नुसार वाह्य का जीवन नहीं बनता। फिर भी अन्तर में परम रमणीय उन्नत विचार हो सकते हैं। दुनियाँ में सब कुछ कार्य-कारण के नियम से चलता, तो भगवान को कोई तकलीफ नहीं देनी पड़ती । आरोग्यवान शरीर में आरोग्यवान मन हो, इस सामान्य नियम के लिये असंख्य अपवाद हुये हैं और होंगे। द्विवेदी जी संसार में बरतने वाले सामान्य जनों के लिये अत्यंत प्रेम रखकर, चित्त में उनके लिये पक्षपात रखकर सर्वोत्तम साहित्य का सृजन करने वाले कालजयी रचनाकार हैं – उनमें मानवीय संवेदना के लिये विकारों से परिपूर्ण निर्लिप्तता है। उनमें बुखार के प्रति हमदर्दी दिखाने वाले वैद्य का लक्षण है। बुखार को ठीक पहचान कर उसके निवारण के लिये दवा भी बताते हैं-
‘‘डरना किसी से भी नहीं । लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं।’’
‘‘जो मेरा सत्य है वह यदि वस्तुत: सत्य है, तो वह सारे जगत का सत्य है, व्यवहार का सत्य है, परमार्थ का सत्य है – त्रिकाल का सत्य है।’’
‘‘देख बाबा, इस ब्रह्माण्ड का प्रत्येक अणु देवता है, त्रिपुर सुन्दरी ने जिस रूप में तुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है, उसी की पूजा कर।’’ (बाणभट्ट की आत्मकथा)
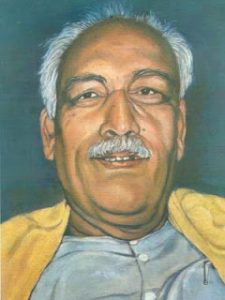 श्री रामदरश मिश्र ने कहा है- ‘‘आखिर सर्जना है क्या ? वह मनुष्य के भावों, संवेदनाओं और विचारों की एक कलात्मक अन्विति है। लेकिन पंडित जी की सर्जना यहीं रुकती नहीं , वे इससे बड़ी सर्जना करते हैं- वह है मानवीय जिजीविषा, विश्वास और मूल्यों की सर्जना। उनके शोध भी, उनकी आलोचना भी, उनके उपन्यास भी, उनके निबंध भी, उनके भाषण भी, उनकी बातचीत भी, उनका व्यवहार भी उसी मनुष्य की खोज और सृष्टि करते हैं जो गतिशील है, जो अपनी अपार जिजीविषा को लिये हुये इतिहास की दुर्गम घाटियाँ पार करता आ रहा है।……वे मानव धर्म की स्थापना मनुष्य के आदर्शों का सरलीकरण करके नहीं करते, उसे उसके द्वंद्व में देखते हैं। मनुष्य के भीतर पशु और देवता का द्वंद्व चलता रहता है, चलता आ रहा है। उसके भीतर की प्राकृतिक पशुता बार-बार सिर उठाती है किन्तु उसका अर्जित देवत्व बार-बार उसे नीचे ढकेलता है। नाखून पशुता की निशानी हैं। नाखून बार-बार बढ़ते हैं, मनुष्य बार-बार उन्हें काटता है। वह नहीं चाहता कि उसकी पशुता उसपर हावी हो जाय। नाखून के बढ़ने और काटने का संघर्ष लगातार चला आ रहा है और पंडित जी विश्वास व्यक्त करते हैं कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य एक दिन इन्हें काटकर ही रहेगा।
श्री रामदरश मिश्र ने कहा है- ‘‘आखिर सर्जना है क्या ? वह मनुष्य के भावों, संवेदनाओं और विचारों की एक कलात्मक अन्विति है। लेकिन पंडित जी की सर्जना यहीं रुकती नहीं , वे इससे बड़ी सर्जना करते हैं- वह है मानवीय जिजीविषा, विश्वास और मूल्यों की सर्जना। उनके शोध भी, उनकी आलोचना भी, उनके उपन्यास भी, उनके निबंध भी, उनके भाषण भी, उनकी बातचीत भी, उनका व्यवहार भी उसी मनुष्य की खोज और सृष्टि करते हैं जो गतिशील है, जो अपनी अपार जिजीविषा को लिये हुये इतिहास की दुर्गम घाटियाँ पार करता आ रहा है।……वे मानव धर्म की स्थापना मनुष्य के आदर्शों का सरलीकरण करके नहीं करते, उसे उसके द्वंद्व में देखते हैं। मनुष्य के भीतर पशु और देवता का द्वंद्व चलता रहता है, चलता आ रहा है। उसके भीतर की प्राकृतिक पशुता बार-बार सिर उठाती है किन्तु उसका अर्जित देवत्व बार-बार उसे नीचे ढकेलता है। नाखून पशुता की निशानी हैं। नाखून बार-बार बढ़ते हैं, मनुष्य बार-बार उन्हें काटता है। वह नहीं चाहता कि उसकी पशुता उसपर हावी हो जाय। नाखून के बढ़ने और काटने का संघर्ष लगातार चला आ रहा है और पंडित जी विश्वास व्यक्त करते हैं कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य एक दिन इन्हें काटकर ही रहेगा।
द्विवेदी जी मानवीय संवेदना के ‘भावानुभावव्यभिचारीभावसंयोगात्रसनिष्पित्त:’ के स्वयंसिद्ध रसवादी साहित्यकार हैं- “There is always a difference between an eager man wanting to read a book and a tired man wanting a book to read”.
हजारी प्रसाद जी समय को आक्रांत करते हैं, समय काटते नहीं। मानव संवेदना की किताब का इतना उत्सुक वाचक हिन्दी साहित्य में तो दुर्लभ ही है, विश्व साहित्य में भी शायद विरला ही मिले। उनके साहित्य में वस्तुनिष्ठा है, जीवन निष्ठा है और साथ-साथ लोकनिष्ठा है। द्विवेदी जी मानवीय संवेदना को समेटे हुये जब मनुष्य और सृष्टि का स्पर्श करते हैं तो जड़ वस्तु जड़ नहीं रह जाती और मनुष्य निरीह प्राणी नहीं रह जाता-
‘‘जीना चाहते हो? कठोर पाषाण को भेदकर, पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो; वायुमण्डल को चूसकर, झंझा-तूफान को रगड़कर, अपना प्राप्य वसूल लो; आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है –
भित्वा पाषाणपिठरं छित्वा प्राभंजनीं व्यथाम्
पीत्वा पातालपानीयं कुटजश्र्चुम्बते नभ: ।
दुरन्त जीवन-शक्ति है! कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है। लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिन्दगी में, मन ढाल दो जीवनरस के उपकरणों में।’’यह एक अनूठी कला है, एक निराली रसिकता है, जिसे हजारी प्रसाद जी ने आत्मसात किया।
मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है में यह कहते हुये कि ‘साहित्य केवल बुद्धि विलास नहीं है, वह जीवन की उपेक्षा करके नहीं रह सकता’, उन्होंने यह संवेदित कर दिया है –‘‘साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम सारे बाह्य जगत् को असुन्दर छोड़कर सौन्दर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। सुन्दरता सामंजस्य का नाम है। जिस दुनिया में छोटाई और बड़ाई में, धनी और निर्धन में, ज्ञानी और अज्ञानी में आकाश-पाताल का अंतर हो, वह दुनिया बाह्य सामंजस्यमय नहीं कही जा सकती और इसीलिये वह सुन्दर भी नहीं है। इस बाह्य असुन्दरता के ‘ढूह’ में खड़े होकर आन्तरिक सौन्दर्य की उपासना नहीं हो सकती। हमें उस बाह्य असौन्दर्य को देखना ही पड़ेगा। निरन्न, निर्वसन जनता के बीच खड़े होकर आप परियों के सौन्दर्य-लोक की कल्पना नहीं कर सकते। साहित्य सुन्दर का उपासक है, इसीलिये साहित्यिक को असामंजस्य को दूर करने का प्रयत्न पहले करना होगा, अशिक्षा और कुशिक्षा से लड़ना होगा, भय और ग्लानि से लड़ना होगा। सौन्दर्य और असौन्दर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता। सत्य अपना पूरा मूल्य चाहता है। उसे पाने का सीधा और एकमात्र रास्ता उसकी कीमत चुका देना ही है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है।’’
द्विवेदी जी ‘फ्रायड’ के Homo-Psycologicus (मन:प्रधान मानव) को नहीं जानते। वे ‘मार्क्स’ के Homo-Economicus (अर्थस्य पुरुषोदास) को नहीं पहचानते। वे बुद्धिवादियों के Homo-Shapian (बुद्धिप्रधान मानव) से भी वाकिफ नहीं हैं। वे एक सामान्य समन्वित मानव की सावित इन्सान की जिन्दगी का जायका पहचानते हैं। उनका रचनाकार जिजीविषा में मशगूल है और यही उनकी मानवीय संवेदना की यथार्थ वैज्ञानिकता है। द्विवेदी जी अपनी रचना में जीवन की सुगंध का अनुभव करना चाहते हैं, जीवन की प्रतिष्ठा देखना चाहते हैं। उपनिषद का अभिवचन है- ‘‘अन्नमयं हियोम्यमन: आपोमया: प्राणा: तेजोमय वाक् ।’’ मनुष्य का तेज उसकी वाणी में प्रकट होता है। वह तेज हृदय की भावना से आता है, जीवन की प्रतीतियों से उत्पन्न होता है। ये प्रतीतियाँ जितनी व्यापक और उदात्त होंगी, उनका आशय जितना भव्य और सुन्दर होगा, उतना सुमांगल्य और सौमनस्य सिद्ध होगा। श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी’ ने लिखा है कि –
‘‘जिन लोगों ने द्विवेदी जी को भाषण देते हुये देखा होगा उन्होंने खुद उनके व्यक्तित्व में भी इस छटपटाहट को जरूर लक्ष्य किया होेगा।……मनुष्य द्विवेदी जी की दृष्टि में चित् का स्फुरण है। इस मनुष्य में उनकी आस्था कभी खंडित नहीं होती। वे मनुष्य की जय-यात्रा में अखंड विश्वास रखते हैं।’’ मानवीय संवेदना के इस चितेरे को उस साहित्य को साहित्य कहने में ही संकोच होता है ‘जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता, परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुखकातर और संवेदनशील न बना सके।’’
जैनेन्द्र कुमार ने कहा है कि,‘‘मुझको सूझता है कि साहित्य वह है, जिसमें हित सत् के साथ है। ‘हित’ के साथ जो ‘स’ लगा है, उसे सत् का प्रतीक हम मान लें। सत् और हित इन दोनों को साथ रखना बड़ी कला है। साहित्य की और शायद जीवन की कला वही है।’’ द्विवेदी जी ने मानवीय संवेदना के प्रस्तुतीकरण में सच में ही ‘सत्’ को ‘हित’ के साथ बनाये रखा है, और यह भाव अनन्त काल तक हमें संवेदित करता रहेगा, क्योंकि साहित्य तो कभीं असमर्थ हुआ नहीं है, हो नहीं सकता। जीवन निष्ठा और साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में एकरूप हो गये हैं। मानवीय संवेदना की चित्त में जो गहरी अनुभूति हुयी है, वह भाषा में सुन्दर रूप लेकर अपनी नित्यता को प्रतिष्ठित करना चाहती है। श्री नामवर जी ने इस तथ्य को बड़ी सदाशयता से स्वीकार किया है –
‘‘प्रसाद जी की श्रद्धा ने तो अपनी स्मिति रेखा से ज्ञान, इच्छा और क्रिया के त्रिपुर को ही आकाश में एकजुट किया था, द्विवेदी जी की सर्जनात्मक कल्पना तो जाने कितनी असम्बद्ध वस्तुओं को एक सूत्र में बाँधती चलती है।’’……‘‘आशय यह है कि वे ‘कोई तैयार सत्य उठाकर हमारे हाथ पर नहीं धरते।’’ जो कुछ भी है वह अपना अनुभूत सत्य। गहरी पीड़ा के बीच से निकले कुछ अनुभव-कण। और ऐसे चमकते हुए कण द्विवेदी जी के निबंधों में यत्र-तत्र-सर्वत्र बिखरे पड़े हैं – कहीं फूलों के ढेर में और कहीं धूल या राख की राशि में।’’(हजारी प्रसाद द्विवेदी:संकलित निबंध : भूमिका)
निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी उस कोटि के रचनाकार हैं जिन्होंने आगत विगत अनागत मानव की संवेदना के हार में गुंथे पुष्पों को अपनी स्वकीय जीवनानुभूति का रस दिया है। ‘विचार-प्रवाह’ के ‘मानव-सत्य’ शीर्षक निबंध में उन्होंने लिखा है –
‘‘जिस काव्य या नाटक या उपन्यास के पढ़ने से मनुष्य में अपने छोटे संकीर्ण स्वार्थों के बन्धन से मुक्त होने की प्रेरणा नहीं मिलती तथा ‘महान एक’ की अनुभूति के साथ अपने-आपको दलित द्राक्षा के समान निचोड़ कर ‘सर्वस्य मूलनिषेचनं’ के प्रति तीव्र आकांक्षा नहीं जाग उठती, वह काव्य और वह नाट्य और वह उपन्यास दो कौड़ी के मोल का भी नहीं है।’’
‘चारु-चन्द्रलेख’ में उन्होंने अक्षोभ्य भैरव से कहलवाया है – ‘‘देख रे, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र हर समय साथ-साथ नहीं चलते। देवी के चरणों में सिर रखकर शपथ कर कि तू सीधे जनता से सम्पर्क रखेगा, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं मानेगा, धरती को बपौती नहीं धरोहर समझेगा, सामन्ती प्रथा का उच्छेद करेगा। ऐसा करके ही तू वीर विक्रमादित्य की परम्परा का उत्तराधिकारी होगा।’’
निश्चय ही श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी मानव संवेदना के अप्रतिम स्रष्टा हैं, जैसा कवि चण्डीदास ने दुहराया –
‘‘शुनह मानुषभाइ
सबार ऊपरे मानुष सत्य
ताहार ऊपरे नाइ।’’

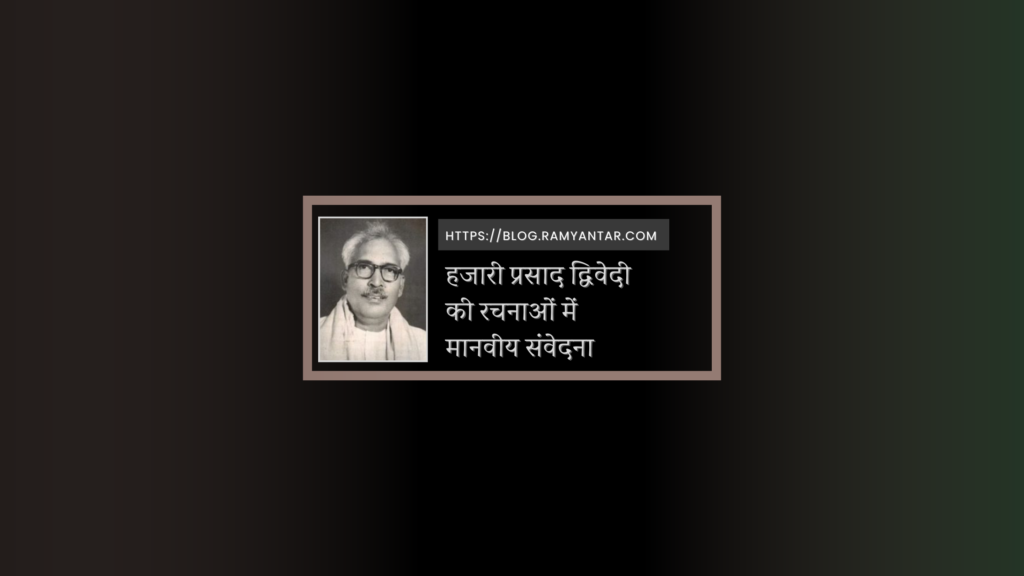





बहुत ही सुन्दर लेख।ऐसे लेखों की एक सिरीज जारी रखते तो अच्छा होता.और इसमें आप समर्थ हैं।आभार।
ज्ञानवर्धक, संतुलित और प्रशंसनीय आलेख।
सादर
श्यामल सुमन
09955373288
http://www.manoramsuman.blogspot.com
shyamalsuman@gmail.com
हिन्दी साहित्याकाश के ज्वाजल्यमान नक्षत्र रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्मदिवस पर आपका यह श्रद्धांजलि आलेख मन को भाया -अपने लेखन से आपने उनकी परम्परा कायम रखी है यह हिन्दी ब्लागजगत के लिए गौरव की बात है -यह नीर क्षीर विवेक कायम रहे ! इस महापुरुष को शत शत नमन !
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदीजी की मानवीय संवेदना को दर्शाता यह लेख अद्भुत है ..बल्कि यूं कहूँ की इस बहाने आपने अपनी मानवीयता को भी प्रमाणित किया है ..इस लेख लो कई बार पढना होगा..ऐसे ही लिखते रहें…बहुत बहुत बधाई और शुभकामनायें..!!
कृपया "लो" को "को" पढें
द्विवेदी जी अद्भुत लेखक थे। उनके कई निबंध और उपन्यास दोबारा-तिबारा पढ़े हैं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है-इसके तो शीर्षक पर ही मुग्ध होता रहता हूं मैं।
आपने बढ़िया लिखा है।
सुन्दर लेख! आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में यह लिखकर बहुत अच्छा काम किया।
आचार्य द्विवेदी जी के लिए यह कहना कि वे ‘फ्रायड’ के Homo-Psycologicus (मन:प्रधान मानव) को नहीं जानते। वे ‘मार्क्स’ के Homo-Economicus (अर्थस्य पुरुषोदास) को नहीं पहचानते। वे बुद्धिवादियों के Homo-Shapian (बुद्धिप्रधान मानव) से भी वाकिफ नहीं हैं; उचित नहीं लगता। वे तीनों को जानते हैं और उन्हें जान समझ कर ही अपने साहित्य संसार में एक नए मनुष्य की रचना करते हैं। मुझे तो हिन्दी साहित्य में उन से अधिक जाना-बूझा साहित्यकार दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। उन के बारे में लिख कर आपने महत्कार्य किया है। उन के बारे में और अधिक लिखे जाने की आवश्यकता है।
द्विवेदीजी के बारे मे आपका लिखा हुआ पढना बहुत ही अच्छा लगा . आभार आपका. इस तरह का लेखन आप सतत करते रहे , यही प्रार्थना है.
रामराम.
बहुत सुन्दर ग्यानवर्द्धक आलेख के लिये धन्यवाद
प्रशंसनीय लेख!
—
ना लाओ ज़माने को तेरे-मेरे बीच
bahut hi gyanvardhak lekh ……badhayi
bahut hi sundar janakari …..bahut bahut shubhkaamana……….
आ० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी पर गवेष्णात्मक शैली मे लिखा आपका लेख द्विवेदी जी की ही शैली प्रतीत हो रहा है। बहुत अच्छा! संग्रहणीय!
द्विवेदीजी के निबंधों के साथ-साथ उपन्यास भी पढ़े हैं। शुद्ध और क्लिष्ट भाषा में अर्थ और शब्द की आलंकारिकता अद्भुत!
Is gambheer charchaa ke liye Bahut bahut badhaayi.
( Treasurer-S. T. )
HAJARI JEE KE RACHANAO KO SAT SAT NAMAN
द्विवेदी जी की रचना – नाखून क्यों बढ़ते हैं – ने मुझे बचपन में बहुत प्रभावित किया था। और उसके बाद तो उनकी लेखनी से अब तक चमत्कृत होता रहा हूं!
श्रद्धांजलि।