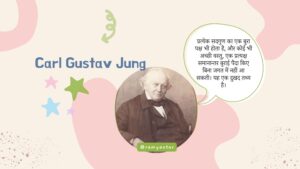शान्ति पर्व पढ़ गया। किसी पुस्तक को पढ़ कर चुपचाप मन ही मन संवाद की आदत है। पहली बार यह बातचीत बाहर आने को मचली। किसे पड़ी है समीक्षा की, इस कविताई को पढ़कर। पर हाथ में लीजिए वरिष्ठ कवि,आलोचक और संपादक आशीष त्रिपाठी का यह कविता संग्रह। जीवन और जगत, मन और आत्मा, प्रेम और साहचर्य तथा समय और समाज जैसे विषयों की चतुर्सरणी आ सिमटती है इस काव्य-सिन्धु में। शांति पर्व कवि का दूसरा काव्य-संग्रह है, पर मेरे लिए पहला है। यह काव्य संग्रह राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। समीक्षा और विवेचना की परिपाटी से बिलकुल अलग कविता को पढ़कर मन में जो निखर-निथर गया, उसे ही कहना हेतु है।
संग्रह की ‘सच मानो’ समूह की एक काव्यात्मक स्फूर्ति ‘एक सुबह अस्पताल’ है। सितम्बर मास, सरकारी अस्पताल का जनरल भर्ती वार्ड। अस्त-व्यस्त रोग शैया पर निढाल पड़ी वार्धक्य दिशि का आमंत्रण पढ़ती रुग्णा शिशु वत्सला माँ। घेर-घेर कर खड़े स्वजन-परिजन। पश्चाताप का पुरश्चरण करती फटी-फटी आँखों वाली रुग्ण की उश्वासें और इसी बीच धक्कामुक्की कर घुसी कौमार पीठिका पर आसीन डबडबायी आँखों वाली विह्वला एक बालिका। इतस्ततः चक्रमण करती घायल मृगशावकी के नयन गंगा यमुना हो गए हैं। वह भी ऐसी कि मार खाकर भी न बोली। पत्नी का आश्चर्य और पति का शून्यावलोकन- यह युगपत समीकरण भाजक-भाज्य बनकर कलेजा कचोट रहा है। काँख की गुदगुदी मुख का वमन बन गई है।

सच मानो ऐसी ही होती है किसी सरकारी अस्पताल की सामान्य व्याप्ति। सच मानो ऐसा ही होता है एक सुबह अस्पताल का कोई सितम्बर। सच मानो ऐसी ही होती है असहाय स्वजनों की भटकती आहें। सच मानो ऐसी ही होती है रुग्णा के रागरंजिता समिधा की आहुति। सच मानो ऐसी ही होती है किसी की आँखों से झरे अश्रुबिन्दु जैसी बालिका की अनबोली डबडबायी आँखें, और सच मानो ऐसा ही होता है मलिन बिस्तर के सिरहाने-पायदाने परिक्रमा करता कवि का संचारी भाव। ‘एक सुबह अस्पताल’ यथार्थ से भी यथार्थ की हड्डी चुन लेने वाली कविता है।
एक बड़ी ही मार्मिक कविता है, ‘दूध पीते बच्चे को देखकर’। यों तो इस संग्रह की ‘जीना’ ‘पुरवा’, ‘कलयुग’, ‘काला सूर्य’, कालिदास’, ‘क्षमा में जुड़े हैं मेरे हाथ’, ‘गहनों की दुकान पर’, ‘तुम्हारी याद’ और ‘तुम्हारा जाना’ जैसी अनेकों निराली रचनाएँ हैं जिनकी तासीर बहुत गर्म है और वे अलग से विवेच्य हैं, किन्तु सच मानो तो ‘दूध पीते बच्चे को देखकर’ इस संग्रह की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है-
‘स्तनों को अपने कोमल होठों के बीच दबाये
दूध की धार खींचता
वह मूँद लेता है अपनी आँखें
जैसे महासुख तृप्ति में नहीं
तृप्ति की प्रक्रिया में है।”
इन पंक्तियों में एक अनुत्तरा झंकृति है। स्तन खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, ततः किम्! महासुख तृप्ति में नहीं तृप्ति की प्रक्रिया में है, ऐसा क्यों? इसलिए न कि गतिमत्यता ही जीवन है! दूध पीते बछडे की पीठ चाटती पयोधरा धेनु जिसका रोम-रोम दुग्धमय हो गया है, जिसकी आँखें बन्द हैं! शिशु जो स्तनपात निरत है, उसकी आँखें बन्द हैं। कुतिया की सूखी अठली को चिचोरते पिल्लों की आँखें बन्द हैं, क्यों? बन्द आँखों को गति का ख़याल कहाँ! गति तो पुनरावर्तन है, अगति तृप्ति है। छाती खींचता बालक मुँह पर दूध की धार झेलकर हँसता है, यह तृप्ति का ही आस्वाद है। ‘पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते’। धाय माँ की मजबूरी भी भजनफल में तृप्ति ही है। स्रवित पय पयोधरों से अधर का स्पर्श ही तृप्ति है। अन्यथा विविक्त संगी मुनियों ने इसी लिए यों ही नहीं कहा था- मातुः पयोधर रसं न पुनः पिवन्ति।’ इस पयःपान कि अनबूझ पहेली सुलझाने में कवि की भावयित्री प्रतिभा अभी और अनेकों पृष्ठ रंगेगी।
मैं इस कविता के सम्मोहन में हूँ। भाव के स्तर पर वात्सल्य के स्पर्श से निथरती करुणा इस कविता मे स्मृति का स्पर्श पाकर विचारों की धुकधुकी में समा जाती है। कवि परम्परा और समय से दो चार होता है, विडम्बनाओं का स्वीकार विचित्र है उसके लिए-
“मनुष्य की महान जय यात्रा की कहानी
दरअसल शुरु होती है यहीं से
दो, तीन या चार थनों के दुह लिए जाने का स्वीकार ही है
सभ्यता की पहली मंजिल”
और अबूझ है धरती का अनन्तकाल से इसे चुपचाप सहना –
“इस दूध पीते बच्चे को देखते
मेरी आँखों में तैरती है धरती
एक गाय की तरह विवश
सहती अनन्तकाल से
दो, तीन या चार थनों का दुह लिया जाना
चुपचाप”
संग्रह की एक विलक्षण लम्बी कविता है ‘काला सूर्य’। यह ‘काला सूर्य’ कविता विपरीत प्रत्यंगिरा स्तोत्र का अखंड पाठ कर रही है।
‘आकाश है नीला/ पर दीखता है अभीं काला’
इसी सूर्य के ही कारण। आकाश क्षय रोगी है, बल वीर्य विहीन। काला सूर्य ‘ मृगपति सरिस अशंक’ उसी आकाश वीथि में ताण्डव मचाए है। दमकता है, चमकता है, आँखों में अन्धेपन की अविश्रान्त रतौंधी रच देता है। नव सर्जित सौर्य मण्डल में आकाश गंगा की परिक्रमा बीच अनिवार्य उछलकूद मचाता है। ग्रहण ग्रस्त न होने की कठिन व्यूह रचना कर ली है। गेरुआ, सफेद, पीला- सब रंग उसकी काली कामरी में लिपट कर काला-काला-काला की थपोड़ी बजा रहे हैं।
उजला सूर्य, उजली ऋचायें, उजले ऋषि, उजले मंत्र सब अतिसार के रोगी हो गए हैं और वमन विरेचन की ऐंठनदार प्रक्रिया में उलझकर हाथ पाँव पटक रहे हैं। फटी-फटी आँखें पूछती हैं – ‘उगा ही क्यों ऐसा सूर्य!
“पराया बनाने वाली ध्वनियाँ
दबंगों सी घूम रही हैं
चीखते चिल्लाते धमकाते”
कितना बलात्कार करेंगी ये! ऐसे शील-हरण का शठ सौन्दर्य अब बर्दास्त के बाहर है।
कवि कहता है-
“तेजस्वी काले सूर्य की अभ्यर्थना में
खड़े हैं हम
……………
भागता हूँ
भागता ही जाता हूँ बेबस
कहीं मिले कोई दृश्य
कोई छुअन
कोई बोल”
इतना लाचार, इतना बेचारा, इतना बेबस! आँखें भरती हैं जब कवि अपनी आहों के शब्द विन्यास की अन्तिम कड़ी में पीठिका सँवारता है –
“आत्मा का उजास
किसी पर्वत की खोह में एक शैतानी संदूक में बंद है”
तनिक दृष्टि बदलें। पूरी की पूरी कविता ही द्वंद्व समास है। कृष्ण ने कहा था न कि समासों में मैं द्वंद्व हूँ। ‘चार्थे द्वंद्वः”। यह भी और वह भी। यह काले सूर्य का क्षैतिज पसारा जो दृश्य है, pessimism की ठठेरी सँजोये लुढ़क जायेगा अतलान्त महासागर में। आत्मा के कालकूट को मर्दित कर संजीवन अमृत का कलश लिए धन्वंतरि आने ही वाला है। आत्मा तो उसे ही आत्मसात करेगी। छटपटाता बिलखाता भाग खड़ा होगा काला सूर्य। ‘तमस्तदासीत गहनं गभीरं की यवनिका छिन्न भिन्न होगी, होगी और ‘यस्तस्य पारेभि विराजते विभुः’ का विरोचन निकलने ही वाला है, निकलने ही वाला है। कवि की कसकती आत्मा वाह्य शब्दों का धोबियापाट भले ही लगा रही हो, पर मल्लयुद्ध में कुन्तीसुर की विजय सुनिश्चित है। हार जाएगा गांधारी का बेटा।
कविता अपनी मार्मिकता में इतना कुरेद रही है कि नींद उड़ जाती है।
आशीष त्रिपाठी की कविताई की मनोगति न तो मंदाक्रान्ता है न द्रुत विलंबित। न तो वसंत तिलका है न शिखरिणी। इन्द्रवज्रा भी नहीं। हाँ, शार्दूल विक्रीड़ित है। विहंगावलोकन नहीं, सिंहावलोकन। सूक्ष्मता से प्रत्येक भाव, भावना और विचारों का अवलोकन और अभिव्यक्ति में अनूठे संयम से प्रभावपूर्ण प्रकटन, यह दुर्लभ युति सहज सुलभ है आशीष त्रिपाठी की कविताओं में।
शान्ति पर्व ठिठक ठिठक कर पढ़ने की कविता की क़िताब है, क्योंकि हर ठिठकन पाठक को भाव, विचार, भाषा और अभिव्यक्ति का अनोखा वैभव साक्षात करने का अवसर देती है। बस इतना ही।