अपने नाटक ’करुणावतार बुद्ध’ की अगली कड़ी जानबूझ कर प्रस्तुत नहीं कर रहा । कारण, ब्लॉग-जगत का मौलिक गुण जो किसी भी इतनी दीर्घ प्रविष्टि को निरन्तर पढ़ने का अभ्यस्त नहीं । पहले इस नाटक को एक निश्चित स्थान पर ले जाकर अगली एक-दो प्रविष्टियों में समाप्त करने का विचार था, इसीलिये जल्दी-जल्दी पहली तीन प्रविष्टियाँ आ गयीं (फिर अरविन्द जी ने हड़काया) । पर थोड़ी तन्मयता और सुधी पाठक जन की सहज स्वीकार्यता ने इसे कुछ और दूर तक ले जाने का संकल्प भरा है । इनकी अत्यधिक प्रेरणा भी रही है कारक । तो निवेदन यही कि अब यह नाटक प्रत्येक रविवार को प्रस्तुत किया जा सकेगा – आप स्नेह दें, सम्बल दें । साभार ….।
एक लम्बी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ – दो तीन प्रविष्टियों में पूरी होगी- अपनी नहीं, पानू खोलिया जी की । ज्ञानोदय (नया ज्ञानोदय नहीं) के पुराने अंकों को पढ़ते आँखें ठहर गयीं, फिर मन भी, संवेदना भी, चिंतन भी । पारायण करें (मुझे लम्बी-लम्बी प्रविष्टियाँ इन दिनों प्रस्तुत करने के लिये निन्दित न करें) –
पराजितों का उत्सव : एक आदिम सन्दर्भ
नहीं जानता –
 हमारे अन्दर होती है कोई आत्मा : शुद्ध-बुद्ध
हमारे अन्दर होती है कोई आत्मा : शुद्ध-बुद्ध होता है ब्रह्म का स्वरूप कोई : चेतन ?
कोई मोक्ष-पद ?
नहीं जानता ।
जानता हूँ लेकिन –
हर आदमी के …आदमी के अन्दर
के अन्दर, के अन्दर, के अन्दर, के अन्दर
– बावजूद तमाम करुणा, संवेदनशीलता, प्रभावितता,
सच्ची सहानुभूति और विगलितता के
– और बावजूद खुली आँखों, कानों, नाक और जीभ
और स्पर्शिततायुक्त एक त्वचा के –
एक और आदमी पैठा है, बैठा है…जीवन्त ।
समाधिस्थ आदमी वह, मुक्त हंस ।
सारे प्रभावों से मुक्त । शुद्ध-बुद्ध-चित्….निर्विकार –
वह है । अपने में सम्पूर्ण । निरपेक्ष ।
सारे ’हैं-ओं’ से निरपेक्ष । हम से भी ।
इतने तमाम क्रूड-क्रूर सचों के अन्दर धँसा हुआ
एक क्रूड-क्रूरतम सच ।
बाक़ी दुनिया है माया….झूठ ।
और वह अन्दर के अन्दर, के अन्दर,
के अन्दर, के अन्दर का आदमी –
कि जिसकी आँखें नहीं, कान नहीं, नाक नहीं,
जीभ भी नहीं ही — एक त्वचा है जरूर,
मगर गैंडे की ।
(बिनु पग चलै, सुनै बिनु काना ।
— शायद ।
— शायद नहीं ।)
वरना….
यह कभी नहीं होता कि आप का दर्द
मेरा न होता,
और मेरी चोट आप की न होती ।
नहीं ही होती है मेरी चोट
कभी आप की नहीं ही होती है, और –
आप का दर्द मेरा नहीं ही होता है ।
बिलकुल…बिलकुल ।
वरना कभी नहीं होता —
कि आप के गृहदाह के अंगारे
मेरी अँगीठी की आँच बन जाते ।
बन ही जाते हैं–आप के गृहदाह के अंगारे
मेरी अँगीठी की आँच बन ही जाते हैं
— महकदार,
— दहकदार ।
अगली प्रविष्टि में जारी…..



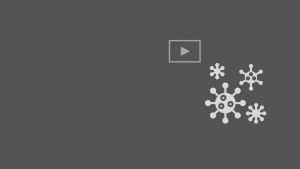



यह एक संचेतना ही तो है जो अखिल ब्रह्माण्ड को आप्लावित किये हुए हैं भले ही वह हमारे अंतरतम के अंतरतम के अंतरतम में कहीं गहरे धसी हो मगर है तो जरूर ही ! और उसे पहचानना ही उन्मुक्त हो जाना है ,निर्वाण का परम पद प्राप्त कर लेना है -और यही अकुलाहट इस काव्याख्यान में सहज ही अनुभूत है !
और महराज,जब घोर वितृष्णा उपजा देने वाली कोई प्रस्तुति हुनर में ऐसी बेजोड़ हो जाय की डराने सी लग जाय तो कोई क्या कहेगा ? बंद कीजिये यह ,प्लीज बंद कीजिये ! खुद साधक के लिए भी ! आप और अभी से यह वैराग्य राग ! कम से कम अपने जीते जी तो मैं ऐसा नहीं करने/होने दूंगा हिमाशु आप के लिए ! एतदर्थ ही था वह आर्तनाद !
हुजूर !
सोचा था बुद्ध पर….लेकिन ठीक है ..
रचनाकार का फैसला अंतिम होता है ……
कविता अच्छी है , यहाँ वैविध्यमय
विश्व के प्रति आत्मचेतस (आत्मकेंद्रित नहीं )
व्यक्ति का चितन पसंद आया …
कवि को आभार … …
बहुत सुंदर आप की कविता, भी दो तीन बार पढेगे फ़िर समझ मै आयेगी.
बहुत बढ़िया रचना . बधाई
परिप्रेक्ष्य नही जानती ..कई दिनों से नेट से दूर हूँ ..पर जैसा की आपकी बातों से प्रतीत होता है कोई सामग्री नेट में आने वाले जिज्ञासुओं के लिए उपहार है ऐसा समझ के मैं लिखती हूँ ..शेष आप स्वयं समझदार है ..आपसे और क्या कह सकती हूँ.
बन ही जाते हैं–आप के गृहदाह के अंगारे
मेरी अँगीठी की आँच बन ही जाते हैं
— महकदार,
— दहकदार ।
दह्कदार तो समझ आया …मगर महकदार भी ….किसी गृहदाह के अंगारे महकदार भी हो सकते है भला ..??….गृहदाह उपन्यास याद हो आया ..
भई हम तो अपने प्रोफाइल माँ बुद्ध को लगाय दिए हैं।
कोरे कागज हैं ये बताने के लिए सब रुचि हटाय दिए हैं।
प्रतीक्षा है:
यशोधरा के पीर की
मार के तान की
सुजाता के खीर की
वीणा के गान की
अंगुलिमाल के कटार की
…. चरैवेति भंते !
___________________________
ब्लॉगरी की भाषा की किनकी 'इनकी' पर बढ़िया लगी।
____________________
ये कविता नरक के पास वाली गली में चल रही है। कहाँ से ढूढ़ लाए – प्रतिद्विन्द्वी ?
छोड़ो भी, हमरा नरक अधिक नारकीय है। लोग आ रहे हैं नरक भोगने बेहूदे निवेदन के बाद भी।
___________________
अगली कविता लम्बी वाली होनी चाहिए – हिमांशु ब्राण्ड। बड़के भैया ये न कहने पाएँ कि हमरी संगति आप को बिगाड़ रही है।
तो प्रकट का अपने अंतरतम से संवाद है.. ये…कविता बहुत ही वैज्ञानिक माध्यम है..खुद के भीतर से उत्तर खींच लेने का..जैसे आटा गूंथते जाओ..तो वो पानी सोखते जाता है और लोई मुलायम पर इंटीग्रेटेड होती जाती है..तो कविता शब्दोत्खनन मांगेगी..और बोध देती जायेगी…!!..इस शुभाशा में..हूँ मै..!!!
सुन्दर! अब जब कविता पूरी हो गयी है तो चारों भाग के लिंक चारो पोस्टों में दे दो ताकि लोग एक से दूसरे भाग तक हर भाग से जा सकें।