प्रस्तुत है पेरू के प्रख्यात लेखक मारिओ वर्गास लोसा के एक महत्वपूर्ण, रोचक लेख The Premature Obituary of the Book: Why Literature का हिन्दी रूपान्तर। ‘लोसा’ साहित्य के लिए आम हो चली इस धारणा पर चिन्तित होते हैं कि साहित्य मूलतः अन्य मनोरंजन माध्यमों की तरह एक मनोरंजन है, जिसके लिए समय और विलासिता दोनों पर्याप्त जरूरी हैं। साहित्य-पठन के निरन्तर ह्रास को भी रेखांकित करता है यह आलेख। इस चिट्ठे पर क्रमशः सम्पूर्ण आलेख हिन्दी रूपांतर के रूप में उपलब्ध होगा । पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठीं कड़ी के बाद प्रस्तुत है सातवीं और अन्तिम कड़ी।
इस प्रकार साहित्य की अवास्तविकताएँ, साहित्य की मिथ्यावादितायें भी मानव की गुह्यतम वास्तविकताओं के ज्ञान के लिए मूल्यवान साधन हैं। जिन सत्यों को यह अभिव्यक्त करता है वह हमेशा खुशामदी करने वाले ही नहीं होते और कभीं-कभीं तो जो हमारी छवि उपन्यासों और कविताओं के दर्पण में उभरती है वह राक्षस की छवि होती है। ऐसा तब होता है जब हम वैसी अप्रिय कामुक प्राणि-हत्याओं के बारे में पढ़ते हैं जिसकी कल्पना डि सेड (Marquis de Sade) ने की है या अंधेरे में की गयी नोंच-चोंथ और निर्मम प्राणहरण की घटनायें जिनसे सचर-मासोक (Sacher-Masoch) और बेटे (Bataille) की अभिशापित पुस्तकें भरीं पड़ी हैं, पढ़ते हैं। उन समयों में ये दर्पण इतने अपराधी, इतने भयंकर हो जाते हैं कि उधर देखना बर्दास्त के बाहर हो जाता है।
फिर भी इनके पन्नों में वर्णित रक्तपात, अवमानना और दुर्दान्त पीड़क घटनायें उतनी अधिक बुरी बातें नहीं हैं, जितना कि यह पता लग जाना कि यह हिंसात्मकता व ज्यादती हमलोगों के लिए अजनबी नहीं है। यह हमारी मानवता का ही बहुत बड़ा हिस्सा है। ये उखाड़ फेंकने को लालायित रहने वाले राक्षस हमारे व्यक्तित्व के अत्यंत अंतरंग अवकाश के गह्वरों में छिपे रहते हैं, और अपने छिपे हुए अंधकारपूर्ण स्थान से वे अनुकूल मौके की तलाश करते रहते हैं ताकि वे स्वयं का अधिकार जमा सकें, अपनी बेकाबू हुई इच्छाओं को लागू कर सकें जिनसे बौद्धिक क्षमता, सामुदायिक एकता और यहाँ तक कि अस्तित्व तक भी मटियामेट हो जाता है।
और यह विज्ञान नहीं था जिसने साहसपूर्ण खोज की मानव मस्तिष्क के इन दुष्कृतिकर स्थानों की और खोज की उस विध्वंसक और आत्मविनाशक शक्ति की जिसको यह रूप देता है। केवल साहित्य ही था जिसने यह खोज की। साहित्य के बिना संसार करीब-करीब अंधा ही बना रहेगा- उन भयानक गहराइयों के प्रति, जिनको जानने-देखने की हमें नितान्त आवश्यकता है।

मारिओ वर्गास लोसा पेरू के चर्चित एवं प्रतिष्ठित साहित्यकार होने के साथ साथ कुशल पत्रकार और राजनीतिज्ञ भी हैं। इन्हें वर्ष २०१० के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ।
जन्म : २८ मार्च, १९३६
स्थान : अरेक्विपा (पेरू)
रचनाएं : द चलेंज–१९५७; हेड्स –१९५९; द सिटी एण्ड द डौग्स- १९६२; द ग्रीन हाउस–१९६६; प्युप्स –१९६७; कन्वर्सेसन्स इन द कैथेड्रल – १९६९; पैंटोजा एण्ड द स्पेशियल -१९७३; आंट जूली अण्ड स्क्रिप्टराइटर-१९७७; द एण्ड ऑफ़ द वर्ल्ड वार-१९८१; मायता हिस्ट्री-१९८४; हू किल्ड पलोमिनो मोलेरो-१९८६;द स्टोरीटेलर-१९८७;प्रेज़ ऑफ़ द स्टेपमदर-१९८८;डेथ इन द एण्डेस-१९९३; आत्मकथा–द शूटिंग फ़िश-१९९३।
बिना साहित्य के यह संसार, यह डरावना संसार, जिसका खाका मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, असभ्य, खतरनाक, असंवेदनशील, भद्दी भाषा बोलने वाला, अज्ञानी, आदिम मनोवृत्तियों से भरा अनुचित भावनाओं और भद्दे भोथरे प्रेम-व्यवहार वाला होगा, और इसका मुख्य-कार्य होगा सुनिश्चितता बनाना और शाश्वत रूप से मानव-जाति का शक्ति के आगे समर्पित हो जाना। इस तरह से विशुद्ध रूप में यह संसार पाशविक संसार भी हो जायेगा। इसमें आदिम मनोभाव ही जीवन के नित्य के क्रियाकलापों का नियमन करेंगे, अस्तित्व के लिये संघर्ष ही कार्यों के सम्पादन का प्रधान गुण होगा, अज्ञात का भय सताता रहेगा, कार्य होंगे भौतिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति के। आध्यात्मिकता के लिये कोई जगह नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस संसार में जीवन में एकरूपता ही बनी रहेगी, जीवन को हमेशा निराशावाद की छाया घेरे रहेगी, यह अनुभव घर किये रहेगा कि जैसा जीवन होना था वह यही है, और यह हमेशा-हमेशा के लिये ऐसा ही रहेगा, और कोई भी कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता।
कोई भी जब ऐसे संसार की कल्पना करता है तो बरबस ही उसके सामने आदिमवासियों का वह चित्र सामने आ जाता है जो बाघाम्बर पहनते थे, जो छोटॆ-छोटे जादुई धार्मिक संप्रदाय के थे, जिनका निवास आधुनिकता के एकदम हाशिए पर लैटिन अमेरिका, ओसीनिया और अफ्रीका में था। लेकिन मेरे मस्तिष्क में एक दूसरी असफलता का चित्र है। जिस भयाकृति की मैं चेतावनी दे रहा हूँ वह अविकास नहीं, अतिविकास की है. तकनीक के विकास और उसके प्रति हमारी अति आज्ञाकारिता के चलते हमें भविष्य में ऐसे समाज की कल्पना दिखायी दे रही है जो कम्प्यूटर की स्क्रीन और स्पीकरों से भरी होगी और बिना पुस्तकों की होगी। बिना पुस्तकों का समाज या यों कहें कि बिना साहित्य का समाज वैसा ही होगा जैसा भौतिक शास्त्र के युग में मध्ययुग की अलकेमी (तुच्छ धातुओं से सोना बनाने की कला) थी, जैसी पुरातन पंथियों की उत्सुकता मीडिया-सभ्यता की चहारदीवारों के लिए मनस्तापग्रस्त अल्पसंख्यकों द्वारा दिखायी जाती थी। मुझे भय है कि अपनी समृद्धि और शक्ति के बावजूद, अपने उच्च जीवन-स्तर और वैज्ञानिक उपलब्धि के बावजूद, यह साइबरनेटिक दुनिया बहुत अधिक असभ्य और पूरी तरह से अनात्मक रहेगी, मानवता पदच्युत हो जायेगी, साहित्य के बाद के मशीनीकरण से स्वतंत्रता छिन जायेगी।
सच में, यह पूरी तरह से असंभव है कि इस तरह का भयावना और अप्रिय कल्पनालोक कभीं आयेगा भी। हमारी कहानी का अंत, हमारे इतिहास की समाप्ति, अभीं लिखी नहीं गयी है, और न इसके बारे में पूर्व सुनिश्चित है। हमें जो होना है, वह पूरी तरह से हमारी परिकल्पना और हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन यदि हमें अपनी कल्पना का भिखमंगापन दूर करने की चाहत है, और इच्छा है कि वह मूल्यवान असंतोष विदा हो जाय जो हमारी संवेदनाओं को सीमित करता है, हमें लचीली और श्रमसाध्य बातचीत की शिक्षा देता है, जो हमारी स्वतंत्रता को कमजोर बना देता है, तो हमें लगना होगा। संक्षेप में कहें तो हमें पढ़ना होगा।
————-समाप्त————-





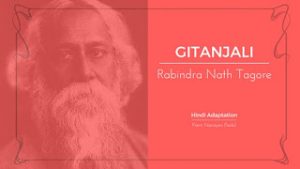

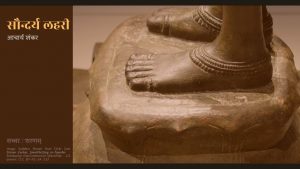
बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं.
बहुत सच कहा, बिना पढ़े तो कल्पनाशीलता भी जबाब दे जाती है।
हिमांशु जी,
हिंदी ब्लॉग जगत को समृद्ध करने के लिए धन्यवाद ; लेखमाला की सारी कड़ियाँ पढ़ने के बाद यही कहूँगा.
चरम विशेषज्ञता के इस युग में एक नयी प्रवृत्ति विकसित हुई है- लेटरल इल्लिटरेसी की . अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र को छोड़कर अन्य के विषय में ज्ञान तो छोडिये सामान्य सूचना भी नहीं है. अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब विद्यालयों में ऐसे अध्यापक होते थे जो दसवीं तक हर विषय पढाने की योग्यता रखते थे. अब तो विषय विशेषज्ञों का ज़माना है. किताबों के प्रति ललक जगाने में अध्यापकों से बड़ी भूमिका किसी की नहीं होती.
बहुत सुन्दर ! बहुत दिनों से अपठित रखा था इस आखिरी कड़ी को.
बहुत ही ज्ञानवर्द्धक रही यह श्रृंखला। आभार।
———
ब्लॉगवाणी: ब्लॉग समीक्षा का एक विनम्र प्रयास।
हाँ, हमें पढ़ना होगा.
पुस्तकों की श्रद्दांजलि मुश्किल है। हाँ कागज़ की श्रद्दांजलि हो अवश्य हो सकती है। पढ़ने में रुचि का अभाव होना चिन्तित कर सकता है परन्तु क्या कल्पना या सन्देश को बाँटने के नवीन साधन अनुपयोगी हैं या प्रतिगामी हैं?
बहुत सुन्दर रही यह शृंखला। लेखक के भय से विनम्र असहमति रखते हुए हुए अमिताभ त्रिपाठी की टिप्पणी से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। धन्यवाद!
जन्माष्टमी की शुभकामनायें!